समान शिक्षा प्रणाली अमीर और गरीब के बीच खाई को पाटने का सेतु है। यह समुदाय-आधारित ऐसी विद्यालय श्रृंखला की कल्पना है, जहाँ अमीर और गरीब के बच्चे एक ही छत के नीचे साथ-साथ पढ़ें, लिखें और खेलें-कूदें। अर्थात् अर्थ, जाति, धर्म, स्थान या लिंग का भेद किए बिना सभी विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाए। सामान्य शिक्षा प्रणाली को समान स्कूल प्रणाली (Common School System) भी कहा जाता है, जिसकी परिकल्पना पड़ोस विद्यालय (Neighborhood School) के रूप में कोठारी आयोग (1964–66) में की गई थी।
प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. अनिल सदगोपाल कहते हैं:
"कोठारी आयोग की अनुशंसा को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और उसका संशोधित रूप (1992) – इन तीनों ने स्वीकारा, लेकिन सरकारों ने अलग-अलग सामाजिक तबकों के लिए अलग-अलग प्रकार की स्कूल व्यवस्थाएं खड़ी करके समान स्कूल व्यवस्था का सरेआम उल्लंघन किया। कोठारी साहब की हार्दिक इच्छा थी कि 1968 की शिक्षा नीति के बाद इसकी पूरी योजना बनाकर उसे लागू किया जाए, पर ऐसा अब तक नहीं हो सका।"
2006 में समाजवादी पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री ने महान समाजवादी नेता एवं चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के "सबकी शिक्षा एक समान" के सिद्धांत को आधार बनाकर बिहार समान शिक्षा प्रणाली आयोग का गठन किया। यह बिहार के लिए अत्यंत गर्व की बात थी कि पहली बार समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने हेतु एक आयोग गठित हुआ।
विदेश सचिव पद से अवकाश प्राप्त श्री मुचकुंद दुबे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉ. मदन मोहन झा को इसका सचिव बनाया गया, और प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. अनिल सदगोपाल को सदस्य मनोनीत किया गया।
आयोग ने 8 जून 2007 को 313 पृष्ठों की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के निर्माण में एससीईआरटी, पटना का अकादमिक सहयोग भी शामिल था। आयोग ने कहा कि आगामी पाँच वर्षों के दौरान राज्य के तमाम प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की पाठ्यचर्या को गांधीवादी शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित कर रूपांतरित किया जाएगा। ज्ञानार्जन, नैतिक मूल्यों का निर्माण और काम के माध्यम से कौशल विकास आयोग का उद्देश्य था।
समान स्कूल प्रणाली शैक्षिक अवसर की समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है, ताकि सभी को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने आवश्यक प्रावधान, स्तर और मानक निर्धारित करने का लक्ष्य बनाया। समान शिक्षा प्रणाली का अर्थ है एक ऐसी आधुनिक, प्रगतिशील, वैज्ञानिक, गुणवत्तापूर्ण और भारत की भू-सांस्कृतिक विविधताओं एवं विभिन्न समुदायों की खूबियों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, जिसमें शिक्षा देना पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी होगी — विद्यालय भवन से लेकर योग्य शिक्षकों तक की व्यवस्था सरकार करेगी, और उस पर नियंत्रण समाज का होगा। इस प्रणाली में पैसे के बल पर शिक्षा खरीदने की छूट किसी को नहीं मिलेगी।
समान स्कूल प्रणाली (बिहार) की अवधारणा एक ऐसी मास्टर की (Master Key) साबित हो सकती थी जिससे कई ताले एक साथ खुल सकते थे — गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भेदभाव। इससे एक नवीन समतामूलक और समरस समाज की स्थापना होती, जो न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श बन सकती थी। "जब तक बिहार की प्रगति नहीं होगी, भारत की प्रगति नहीं होगी।"
दुर्भाग्यवश, इस रिपोर्ट को बिहार विधानमंडल में कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। आयोग के सचिव डॉ. मदन मोहन झा जब तक जीवित रहे, किसी भी तरह से समान स्कूल प्रणाली के कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रहे। परंतु उनके निधन के साथ ही इस युगांतकारी पहल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे बिहार से जो एक सकारात्मक संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए था, वह संभव नहीं हो पाया।
आज भी लोगों को आशा है कि कोई भी क्रांति, यदि होगी, तो वह बिहार से ही शुरू होगी। आज नहीं तो कल, समान शिक्षा प्रणाली जैसी शिक्षा-क्रांति बिहार से ही जन्म लेगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत 25% सीटों पर PPP (Public-Private Partnership) मॉडल के माध्यम से निजी विद्यालयों में प्रवेश का प्रावधान किया गया। जबकि, यदि समान शिक्षा प्रणाली लागू होती तो संभवतः इस अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शिक्षा का अधिकार, वस्तुतः समान शिक्षा प्रणाली का ही एक अंश है।
यह यक्ष प्रश्न है कि आज़ादी के 57 वर्षों बाद भी देश में समान स्कूल प्रणाली क्यों नहीं लागू हो सकी? यदि यह लागू हो जाती, तो विद्यालयी शिक्षा में यह एक क्रांतिकारी कदम होता।
शिक्षा रूपी पौधे का सही 'कल्टीवेशन' समान शिक्षा प्रणाली के बिना अधूरा है। इसके बिना शिक्षा का अधिकार एक मृगतृष्णा बनकर रह जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रारंभ से ही यह प्रावधान था कि राज्य 10 वर्षों की अवधि में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। लेकिन 2002 में किए गए 86वें संविधान संशोधन की धारा 3 के तहत यह दायरा घटाकर 6 वर्ष तक की आयु तक सीमित कर दिया गया, जिससे राज्य की ज़िम्मेदारी घट गई।
1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू तो हुआ, लेकिन आज भी यह सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका है। यदि कानूनी बाध्यता और राजनीतिक इच्छाशक्ति होती, तो देशभर में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता था।
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार केस में जन्म से लेकर जीवनपर्यंत बच्चों के पोषण और शिक्षा की बात की गई थी, परंतु वह याचिका सफल नहीं हो सकी।
यह संतोष की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में 3 से 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की मानी गई है। अच्छे परिणामों के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी।
समान स्कूल प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि चाहे कोई नेता हो या अफसर — सभी को उसी गाँव या मोहल्ले के स्कूल में पढ़ना होगा, जहाँ उनका निवास है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी सांसद या विधायक का बच्चा उसी जर्जर स्कूल में पढ़े जहाँ आम बच्चों को पढ़ना होता है, तो आधारभूत संरचना से लेकर अकादमिक गुणवत्ता तक सब कुछ तेजी से सुधर जाएगा।
सरकारी विद्यालय चकाचक हो जाएंगे, और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यही पड़ोस विद्यालय (Neighbourhood School) की कल्पना है — एक क्रांतिकारी सोच।
इतिहास गवाह है कि 1911 में जब गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने हेतु विधेयक पेश किया था, तो उसे पास नहीं होने दिया गया। दरभंगा महाराज ने तो यह कहकर विरोध किया — "गरीबों के बच्चे यदि पढ़-लिख गए, तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा?"[1]
पैरेटो का 'एलीट वर्ग' और जे. एस. मिल का 'पावर एलीट' आज भी भारत की शिक्षा नीति में बाधक बनते हैं। नीतियां तो बनती हैं, लेकिन वातानुकूलित कमरों में, जिनका ज़मीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं होता।
मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बँटा है — शोषक बुर्जुआ वर्ग और शोषित सर्वहारा वर्ग। यदि बरगद के पेड़ के नीचे नन्हा पौधा लगाया जाए तो क्या वह पनप पाएगा? नहीं — उसे न धूप मिलेगी, न हवा, न पोषण। समाज में अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। छोटे व्यापारी, बड़े पूंजीपतियों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। निजीकरण ने मानो धनाढ्य वर्ग को "कारून" के खजाने की चाबी थमा दी हो — वह बादशाह जिसके खजाने की चाबियाँ 40 ऊँटों पर लाद कर चलती थीं।
अंततः, भुगतना तो आमजन, विशेषकर निम्न और मध्यवर्ग को ही पड़ता है।
डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने जिस समान स्कूल प्रणाली की कल्पना की थी, वह शिक्षा का एक आदर्श बग़ीचा था, परंतु समाज की ठंडी हवाओं और असमान संरचना के कारण उसकी कोपलें कुम्हला गईं। यदि सामाजिक अवरोध न होते, तो यह योजना अब तक एक अधिनियम बन चुकी होती और लागू भी हो चुकी होती।
तब हम सभी मिलकर शंकर शैलेन्द्र की ये पंक्तियाँ गा सकते:
"तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यक़ीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।"
[1] गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक (Compulsory Primary Education Bill) प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य था कि सरकार सभी बच्चों को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करे। किंतु विधेयक को सरकार और कई प्रभावशाली वर्गों के विरोध के कारण पारित नहीं किया गया। हालाँकि यह कहा जाता है कि कुछ जमींदारों ने इस प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया कि यदि गरीब पढ़-लिख गए तो खेतों में काम कौन करेगा, लेकिन दरभंगा महाराज द्वारा ऐसा कोई बयान दिए जाने के प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह उद्धरण अधिकतर लोकप्रचलित कथन के रूप में देखा जाता है, न कि सत्यापित इतिहास के रूप में।


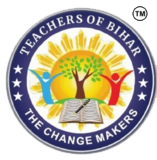









jila baal grih vacancy 2025
ReplyDelete